यों रविवार छुट्टी और आराम का दिन होता है, लेकिन अगर पूछा जाय तो मेरे लिए यह सबसे ज्यादा थकाऊ और पकाऊ दिन होता है। दिन भर बंधुवा मजदूर की तरह चुपचाप हफ्ते भर के घर भर के इकट्टा हुए लत्ते-कपडे, बच्चों के खाने-पीने की फरमाईश पूरी करते-करते कब दिन ढल गया पता नहीं चलता। अभी रविवार के दिन भी जब दिन में थोड़ी फुर्सत मिली तो बच्चों की फरमाईश आइसक्रीम खाने को हुई तो निकल पड़ी बाजार। घर से कुछ दूरी पर सड़क की मरम्मत करते कुछ मजदूर दिखे। उनके पास ही जमीन पर एक ३-४ माह का बच्चा लेटा था, जिसके पास ही उसके भाई-बहन थे। पास बैठी तो भरी दुपहरी में भी मासूम बच्चे की मुस्कान ने मन मोह लिया। मजदूर माँ को कहकर मैं उनके बच्चों को अपने घर ले आयी। अपने बच्चों के साथ-साथ उनको भी जब खाना और आइसक्रीम खिलाई तो मन को गहरी आत्मसंतुष्टि मिली। सभी बच्चों को उस छोटी से जान के साथ खेलते-खिलाते देख सोचने लगी कि हम क्यों नहीं हर समय इन बच्चों सा मासूम दिल रख पाते हैं? क्यों नहीं ऊँच-नीच, जात-पात का भेदभाव भुलाकर मानवता का धर्म निभा पाते हैं? जाने कितने ही विचार मन में कौंध रहे थे। शाम को उनकी माँ के साथ दो घडी बैठकर बतियाना बहुत अच्छा लगा। जब वे ख़ुशी से हँसते-मुस्कराते अपने घर से निकले तो मन में आत्मसंतुष्टि तो थी कि मैंने अपना कुछ तो मानवता का फर्ज निभाया लेकिन उन्हें मैं अपने पास हमेशा नहीं रख सकती इस बात का दुःख हो रहा था। उनके चले जाने के बाद जब मुझे मजदूर दिवस का ख़याल आया तो जाने कितने ही विचार मन में कौंधने लगे।
भारत में मजदूर दिवस मनाना मेरे हिसाब से कोई गौरव की बात नहीं है। क्योंकि आज मजदूरों के हालात बहुत दयनीय है। न इंसाफ मिलता है, न पेटभर भोजन मिलता है और ना ही जीने की आजादी। मुझे तो लगता है कि भारत में मजदूर होने ही नहीं चाहिए क्योंकि मजदूर मजबूर होता है। आज भारत में कृषि से पलायन हो रहा है। आज का किसान अपने बच्चे को न तो किसान बनाना चाहता है और नहीं खुद किसान बना रहना चाहता है। गाँव से वह शहरी चकाचौंध में अपनी सुखमय जिंदगी के सपने देखता है। बस मजदूर (मजबूर) की कहानी यहीं से शुरू होती है। अपने बच्चों को थोडा बहुत पढ़ा-लिखा कर और कभी खुद भी किसानी छोड़ शहर की ओर निकल तो जाता है लेकिन योग्यता, चालाकी और पैसे की चलते हजार दो हजार की नौकरी मजबूरी में कर किसान से मजदूर बन जाता है। जहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं, रात को किसी फुटपाथ पर सो गए तो सुबह सही सलामत जागने की कोई गारंटी नहीं रहती। इनकी बातें हम न तो समाचार पत्र में पढ़ पाते हैं और नहीं इनके नजदीक रह पाते हैं।
तो क्या मजदूर दिवस के दिन उनकी स्थिति सुधारने के बजाय हमारा सिर्फ बड़े-बड़े झंडे-डंडे, पोस्टर आदि लेकर भीड़ जुटाकर भाषण सुनना भर रह गया है? यह बहुत गहन विचार का विषय नहीं है कि जहाँ सामंतवादी सोच के कारण चंद लोगों के पास अकूत धन-दौलत के भण्डार है, वही दूसरी और गरीब मजदूरों के पास दरिद्रता, भूख, उत्पीडन, नैराश्य, अशिक्षा और बीमारी के सिवाय कुछ नहीं है। देश में जिस तीव्र गति से करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उससे चौगुनी मजदूरों की संख्या का बढ़ना एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है नहीं तो और क्या है? आज तमाम सरकारी-गैर सरकारी घोषणाओं, दावों के बीच भी इनकी वास्तविक कहानी आधे पेट भोजन, मिटटी के वर्तन, निकली हुई हड्डियाँ, पीली ऑंखें, सूखीखाल, फोड़ेयुक्त पैर, मुरझाये चेहरे और काली आँखों में गहरी दीनता और निराशा ही बनी हुई है। ऐसे में एक दिनी कार्यक्रम के बाद समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में रहने के बाद यह सोच लेना कि मजदूर दिवस सार्थक रहा, इसे कितना ठीक है? मेरे हिसाब से अगर भारत को वापस सोने की चिडि़या बनाना है तो पहले मजदूर को उसकी बदहाली से मुक्त करना होगा।
तो क्या मजदूर दिवस के दिन उनकी स्थिति सुधारने के बजाय हमारा सिर्फ बड़े-बड़े झंडे-डंडे, पोस्टर आदि लेकर भीड़ जुटाकर भाषण सुनना भर रह गया है? यह बहुत गहन विचार का विषय नहीं है कि जहाँ सामंतवादी सोच के कारण चंद लोगों के पास अकूत धन-दौलत के भण्डार है, वही दूसरी और गरीब मजदूरों के पास दरिद्रता, भूख, उत्पीडन, नैराश्य, अशिक्षा और बीमारी के सिवाय कुछ नहीं है। देश में जिस तीव्र गति से करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उससे चौगुनी मजदूरों की संख्या का बढ़ना एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है नहीं तो और क्या है? आज तमाम सरकारी-गैर सरकारी घोषणाओं, दावों के बीच भी इनकी वास्तविक कहानी आधे पेट भोजन, मिटटी के वर्तन, निकली हुई हड्डियाँ, पीली ऑंखें, सूखीखाल, फोड़ेयुक्त पैर, मुरझाये चेहरे और काली आँखों में गहरी दीनता और निराशा ही बनी हुई है। ऐसे में एक दिनी कार्यक्रम के बाद समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में रहने के बाद यह सोच लेना कि मजदूर दिवस सार्थक रहा, इसे कितना ठीक है? मेरे हिसाब से अगर भारत को वापस सोने की चिडि़या बनाना है तो पहले मजदूर को उसकी बदहाली से मुक्त करना होगा।










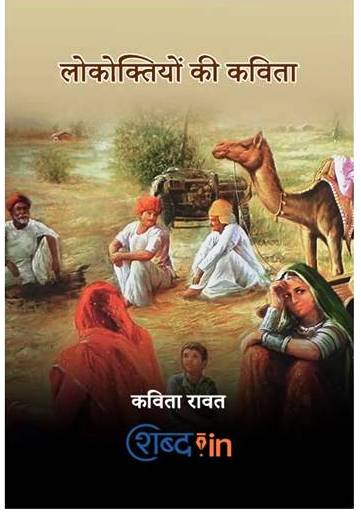



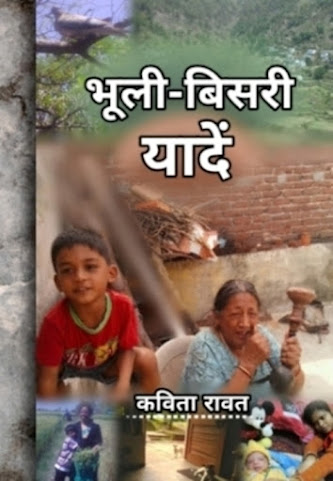


44 टिप्पणियां:
जिस तीव्र गति से करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उससे चौगुनी मजदूरों की संख्या का बढ़ना एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है नहीं तो और क्या है? आज तमाम सरकारी-गैर सरकारी घोषणाओं, दावों के बीच भी इनकी वास्तविक कहानी आधे पेट भोजन, मिटटी के वर्तन, निकली हुई हड्डियाँ, पीली ऑंखें, सूखीखाल, फोड़ेयुक्त पैर, मुरझाये चेहरे और काली आँखों में गहरी दीनता और निराशा ही बनी हुई है।satik lekh ....
bhut gambhir visay pr likha hai......aap aabhnandn ke haqdar he....warna majdur pr kon likh likhta hai!!!!
मजदूर दिवस को याद कर आत्म मंथन और आत्मसंतुष्टि पाने का आपका प्रयास आपके भीतर की गहरी मानवियता को दिखाता है। मजदूर होना और मजदूरी करना कोई गलत बात तो है नहीं कारण दुनिया का प्रत्येक काम करने वाला कार्यरत आदमी मजदूर ही है। बूरी बात है मजदूरों के शोषण की। आप जिस मानवियता से सोच रही है वह सबके दिलों-दिमाग में प्रकाशित हो यहीं अपेक्षा।
सच में बदहाल है मजदूरों का जीवन ....सार्थक लेख
अमीर और गरीब के बीच बढ़ते फासले ने ही इस खूबसूरत दुनिया का बेडा गर्क किया है !
सार्थक चिंतन !
काश ऐसी स्थिति आये कि मजदूर दिवस पर दुख न हो, उत्सव मने।
किसी की मजबूरी और लाचारी का कैसा उत्सव जिसके एक दिन की रोजी उसको भरपेट भोजन नहीं दे पाती उसको उत्सव का मतलब क्या मालूम आज के दिन तो अगर उसको उत्सव मनाना है तो सायद औरो दिनों से जद मेहनत करनी होगी
अगर हमें वाकई इनके लिए कुछ करना है तो हमें इनका आत्मसम्मान वापस लौटना चाहिए ये हमारे लिए मेहनत करते है तब हम इन्हें पैसा देते है हम कोई अहसान नहीं करते है इनपर ,
ये अपना घर बार अपना खेत खलिहान छोड़ कर पैसा कमाने आते है वो भी मेहनत कर के अपना अत्मसम्मान को बेचने नहीं आते
इनको खैरात में सरकार की योजना की जरूरत भी नहीं है और नहीं ऐसी किसी योजना की जिसे इनको नाकारा कर दे इनको तो अपना सम्मान और अपनी मेहनत का दाम चाहिएऔर हमारा प्यार चाहिए
देखा जाये तो हर इन्शान किसी न किसी का मजदूर है फर्क बस नाम और पैसो का है तब मजदूर का नाम मजदूर होना ही नहीं
क्या
होना
चाहिए
ये
हमारे पाठक
बताये तो जद बेहतर है
पर मजदूर नहीं होना चाहिए
mazdoor diwas par ek saarthak saamajik aalekh, shaaririk shram upekshit hai jabki maansik shram ki pau baarah hai! hum apne apne star se sharirik shram ko mahatva pradan karen, uska samman karen aur mazdoor-kisaanon ke samaanta aur behtar jeevan jine k adhikaar ki raksha karen to shayad har mazdoor apne bete ko mehnatkash banana chahega aur humare khet khalihaan bhi bache rahenge, varna aane wala samay bahut mushkil hoga.
मजबूरी ही मजबूर करती मजदूर बनने के लिए ,,,
RECENT POST: मधुशाला,
सच से साक्षात्कार ।
मजदूर दिवस पर अच्छा लेख
सामयिक लेख,
मजदूरों की असल तस्वीर
सच कहा है ... इनकी हलात बड से बदतर होती जा रही है ... दावे खोखले हैं विकास के ...
जब तक देश का मजदूर शशक्त नहीं होगा निर्माण अधूरा रहेगा ...
.......जब तब हमें मजदूरों का सम्मान करना नहीं आएगा तब तक ऐसे दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है ... ..
श्रमिक दिवस पर बेहतरीन उम्दा आलेख ....अनंत शुभकामनायें ..
आपने बहुत ही सुन्दर मुद्दा उठाया है किन्तु मज़दूर और उनके प्रकार, गाँव और शहर के मज़दूर, पढ़े और अनपढ़, उपलब्ध सुविधाओं की सही पूर्ति फिर प्रतिदिन एक नई समस्या, आपने योजना बनाई सौ लोगों के लिए और प्रति सेकण्ड पैदा होने वालों ने इसे प्रतिदिन बढ़ा दिया हम कहते और लिखते रहेगे समाधान मज़दूर के पास है ,,एक गहरी बात आपने कही स्वागतेय
औरत एक ममतामयी ह्रदय रखती है उसका उदाहरण आपने बच्चे को घर लाकर दिया .....
काश हम सब में ऐसी मानवता होती तो न कोई मजदूर होता न कोई मालिक ....
मार्मिक और भावुक
बड़ों से ही सीखे जाते हैं संस्कार
मजदूर दिवस की
उत्कृष्ट प्रस्तुति
विचार कीं अपेक्षा
jyoti-khare.blogspot.in
कहाँ खड़ा है आज का मजदूर------?
जिनके दिल मोम के होते हैं उनके मन में मानवीयता, ममता, सम्वेदना होती है. ऐसे अच्छे लोग मजदूरों की पीड़ा को महसूस करते हैं किंतु इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकें.
जो लोग सक्षम होते हैं, जो हर तरह से मदद करने का सामर्थ्य रखते हैं पता नहीं क्यों पत्थर दिल होते हैं.
कोमल मन की सादगी भरी अभिव्यक्ति अंतर्मन को छू गई.
जिनके दिल मोम के होते हैं उनके मन में मानवीयता, ममता, सम्वेदना होती है. ऐसे अच्छे लोग मजदूरों की पीड़ा को महसूस करते हैं किंतु इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकें.
जो लोग सक्षम होते हैं, जो हर तरह से मदद करने का सामर्थ्य रखते हैं पता नहीं क्यों पत्थर दिल होते हैं.
कोमल मन की सादगी भरी अभिव्यक्ति अंतर्मन को छू गई.
अगर भारत को वापस सोने की चिडि़या बनाना है तो पहले मजदूर को उसकी बदहाली से मुक्त करना होगा...................और इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास के साथ ही व्यक्तिगत प्रयास करने जरुरी हैं ..
..शानदार लेख ....हार्दिक बधाई ..
विचारणीय आलेख।
..शानदार लेख ....हार्दिक बधाई ..
Hakikat ko bayan karne wala lekh hai kavita didi ji...
खुबसूरत और अर्थपूर्ण आलेख हैं!
lateast post मैं कौन हूँ ?
latest post परम्परा
सार्थक आलेख ...
मजदूर दिवस पर सार्थक आलेख .. बधाई ..
शानदार लेख हार्दिक बधाई ..
मजदूरों को भाषण नहीं, पेट भर राशन चाहिए।
सार्थक आलेख !
बहुत ही उम्दा पोस्ट |सुनहरी कलम पर आने हेतु आभार |
श्रमिक दिवस पर बेहतरीन उम्दा आलेख .....कविता जी
मजदूर और मजबूर में दू और बू का फर्क है
मजदूर दिवस पर सार्थक लेखन
बधाई
मजदूरों की दयनीय स्थिति बहुत चिंता जनक है भारत के विकास में...
बेचारे गाँव से शहर की ओर पलायन करते है पर न गाँव न शहर के रहते है बस मजदूर रह जाते है..
काश ऐसी स्थिति आये कि मजदूर दिवस पर दुख न हो,मजदूर दिवस पर सार्थक लेखन।
हर बात के लिये एक दिवस दिखने के लिये अन्यथा बाकी दिन उनकी भलाई याद भी नहीं आती.
कौन समझना चाहे इनको ..
शुभकामनायें !
विचारोत्तेज़क आलेख, काम लेकिन कठिन है, फिर भी एक कदम बढ़े तो सही.
अपने हक़ के लिये लड़ते हुये समर्पित भाव से किसी की मज़बूरी का लाभ न उठा कर अपने श्रम का मूल्य वसूल करें तथा देशं की प्रगति में सहभागी बनेब |
पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अतिथि परिवार की खुशी का अंदाज़ लगाना कठिन नहीं है। गरीबी सचमुच एक अभिशाप है। कमियाँ पहले भी थीं, लेकिन कम से कम धार्मिक भावनाएं तो थीं, जिनके कारण नैतिकता, दया और समाजसेवा का भाव पूरी तरह से मिटा नहीं था। अब तो धर्मसत्ता भी समाप्तप्राय है और मूल-अधिकार व शासन-व्यवस्था का पूर्णाभाव है। यह स्थिति बदलनी ही होगी।
अच्छा लेख
सब दिखावा और बतोल्बाज़ी है | सार्थक लेख | आभार
कभी यहाँ भी पधारें और लेखन भाने पर अनुसरण अथवा टिपण्णी के रूप में स्नेह प्रकट करने की कृपा करें |
Tamasha-E-Zindagi
Tamashaezindagi FB Page
बेहतरीन उम्दा आलेख
एक टिप्पणी भेजें